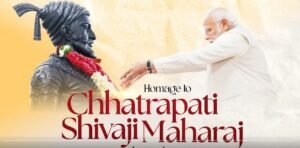Greater Noida:
एक संकट जो असहज रूप से परिचित लगा
इंडिगो में हाल ही में उत्पन्न परिचालन संकट, जिसके कारण भारतीय हवाई अड्डों पर हजारों यात्री फँस गए, को व्यापक रूप से योजना और शासन की विफलता के रूप में देखा गया। पायलटों के विश्राम से संबंधित एक सुरक्षा नियम पहले से मौजूद था, जोखिम भी ज्ञात थे, फिर भी दक्षता और विकास के नाम पर तैयारियों से समझौता कर लिया गया। जब पूरी व्यवस्था चरमरा गई, तो आम नागरिकों को इसकी कीमत चुकानी पड़ी।
इस घटनाक्रम को अस्थिर करने वाली बात केवल उड़ानों का रद्द होना नहीं था। असल बेचैनी इस एहसास से पैदा हुई कि इसके पीछे का सोचने का तरीका कहीं न कहीं बहुत जाना-पहचाना लगा। इंडिगो की चूक कोई अपवाद नहीं थी; यह भारतीय समाज में गहराई तक समाए एक व्यापक मानसिक रवैये का प्रतिबिंब थी।
“इंडिगो क्षण” अब केवल कॉरपोरेट बोर्डरूम तक सीमित नहीं रह गया है। यह हमारे घरों, बाजारों, कार्यस्थलों, कक्षाओं और डिजिटल जीवन में रोज दिखाई देने लगा है।
जब स्वार्थ व्यक्तिगत प्राथमिकता बन जाए
इस नैतिक भटकाव के केंद्र में एक साधारण लेकिन विनाशकारी विचार काम कर रहा है: पहले मेरा लाभ, परिणाम बाद में। यही विचार अनगिनत रोजमर्रा के फैसलों को नियंत्रित करता है। निजी सुविधा के लिए यातायात नियम तोड़े जाते हैं। अधिकार जताते हुए कतारें लाँघ दी जाती हैं। प्रपत्र आधे-अधूरे सच के साथ भरे जाते हैं। बेईमानी को “एडजस्टमेंट” और शॉर्टकट को “व्यावहारिकता” का नाम दे दिया जाता है।
हर कार्रवाई अलग-अलग देखने पर हानिरहित लगती है। लेकिन सामूहिक रूप से यही कार्रवाइयाँ सामाजिक अनुबंध को कमजोर कर देती हैं।
जिस तर्क के सहारे एक बड़ी एयरलाइन बेहद कम परिचालन सुरक्षा-मार्जिन बनाए रखती है, वही सोच तब भी दिखाई देती है जब कोई दुकानदार सामान में मिलावट करता है, बिल्डर सुरक्षा मानकों से समझौता करता है या कोई पेशेवर बिलों में हेरफेर करता है। धारणा एक जैसी रहती है: व्यवस्था इसकी कीमत सह लेगी; भुगतान कोई और करेगा।
हमारी थालियों में ज़हर
शायद रोजमर्रा के नैतिक पतन की सबसे चिंताजनक अभिव्यक्ति उस भोजन में दिखाई देती है जिसे हम खाते हैं। खाद्य पदार्थों में मिलावट अब अपवाद नहीं, बल्कि सामान्य व्यवहार बन चुकी है। पानी या रसायनों से पतला किया गया दूध, कृत्रिम रंगों से मिलाए गए मसाले, अत्यधिक कीटनाशकों से उपचारित सब्जियाँ और नकली डेयरी उत्पाद—ये सब अब चौंकाने वाले खुलासे नहीं, बल्कि बार-बार सामने आने वाली खबरें बन गए हैं।
ये केवल दूर-दराज के कॉरपोरेट अपराध नहीं हैं। इनमें अक्सर वही साधारण व्यापारी और आपूर्तिकर्ता शामिल होते हैं जो उन्हीं समुदायों के बीच रहते हैं जिन्हें वे खतरे में डालते हैं। इसके पीछे मूल प्रेरणा मुनाफे की सुरक्षा होती है। प्रतिस्पर्धा को इसका बहाना बनाया जाता है और परिणामस्वरूप जनस्वास्थ्य से गंभीर समझौता हो जाता है।
इस पूरी प्रवृत्ति को और अधिक परेशान करने वाली बात है—मौन स्वीकृति। उपभोक्ता निजी तौर पर शिकायत तो करते हैं, लेकिन अक्सर जानबूझकर सस्ते विकल्प चुनते रहते हैं, जिससे यह दुष्चक्र लगातार चलता रहता है। किफायती होने के नाम पर नैतिकता छोड़ दी जाती है—और वर्षों बाद जब स्वास्थ्य संबंधी कीमत सामने आती है, तब तक जवाबदेही तय करना लगभग असंभव हो चुका होता है।
संकट से परे सीख
इंडिगो से जुड़ा यह प्रकरण समय के साथ सुर्खियों से ओझल हो जाएगा। उड़ानें सामान्य हो जाएँगी। व्यवस्थाएँ खुद को ढाल लेंगी। लेकिन गहरा सवाल फिर भी बना रहेगा।
– क्या कोई समाज तब फल-फूल सकता है जब विश्वास से लगातार समझौता किया जाता रहे?
– क्या विकास टिकाऊ हो सकता है जब नैतिकता वैकल्पिक बन जाए?
आकाश भले ही असीम हो, पर विश्वास बेहद नाज़ुक होता है। और एक बार जब कोई समाज इसे खो देता है—चाहे वह भोजन हो, दवाएँ हों, शिक्षा हो, सूचना हो या संस्थाएँ—तो निजी लाभ की कोई भी मात्रा सामूहिक व्यवस्था को संभाल कर नहीं रख सकती।
आज भारत को सबसे जरूरी मार्गदर्शन केवल आसमान में नहीं, बल्कि रोजमर्रा के जीवन की नैतिक दिशा और सही–गलत की समझ में चाहिए।